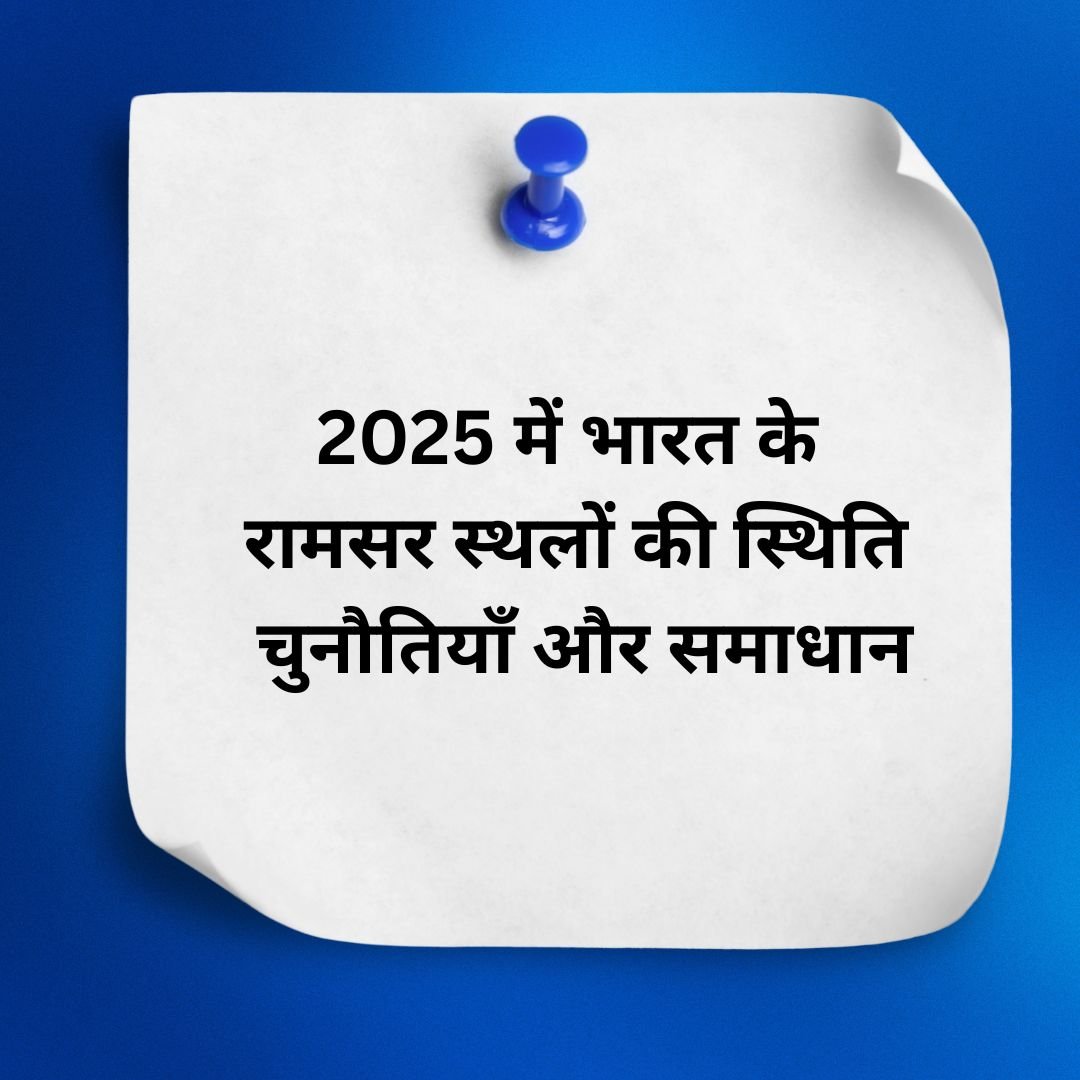Ramsar sites in India 2025
Ramsar sites in India 2025: आर्द्रभूमियाँ (Wetlands) पृथ्वी के सबसे समृद्ध और उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से हैं, जो जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, भू-जल रिचार्ज, कार्बन संग्रहण तथा जैव-विविधता के संरक्षण जैसी अनेक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी सेवाएँ प्रदान करती हैं। इनकी अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व को मान्यता देने हेतु 1971 में रामसर सम्मेलन (Ramsar Convention) सम्पन्न हुआ, जिसमें आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं समुचित उपयोग (wise use) पर वैश्विक सहमति बनी। भारत 1982 में रामसर सम्मेलन का आधिकारिक पक्षकार बना और तभी से देश में चुनी हुई महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों को “रामसर स्थल” घोषित किया जा रहा है। रामसर स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियाँ कहा जाता है, जिनके संरक्षण के लिए संबंधित सरकार अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता जताती है। वर्ष 2025 तक भारत में कुल 91 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं , जिनका संयुक्त क्षेत्रफल लगभग 13.6 लाख हेक्टेयर से अधिक है । हाल ही में जून 2025 में राजस्थान के खीचन (फलोदी) और मेनार (उदयपुर) नामक दो नई आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में जोड़कर देश का कुल आंकड़ा 91 पर पहुँचा । इस अभूतपूर्व वृद्धि के साथ, भारत रामसर स्थलों की संख्या के मामले में एशिया में प्रथम स्थान पर तथा विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है (भारत से अधिक रामसर स्थल केवल यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको में हैं) । तमिलनाडु राज्य वर्तमान में 20 रामसर स्थलों के साथ देश में शीर्ष पर है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 स्थल हैं । भारत के रामसर स्थलों में ऊँचे पहाड़ों की झीलों से लेकर समुद्री तटों के मैंग्रोव, ग्रामीण जलाशयों से लेकर शहरी दलदल तक विविध प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं, जो जैव-विविधता संरक्षण और टिकाऊ उपयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। देश में हाल के वर्षों में रामसर स्थलों की संख्या में तेज वृद्धि देखी गई है – 2014 तक जहाँ केवल 26 रामसर स्थल थे, वहीं 2014 से 2024 के बीच 59 नए स्थल जोड़े गए । यह वृद्धि wetlands के संरक्षण के प्रति नीतिगत प्राथमिकता को दर्शाती है। हालांकि, संख्या में वृद्धि के साथ इन स्थलों की वास्तविक स्थिति और संरक्षण की चुनौतियाँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इस लेख में हम भारत में सभी वर्तमान रामसर स्थलों की राज्यवार सूची, 2022-2025 के बीच जोड़े गए नए स्थलों पर विशेष फोकस, इनके समक्ष पर्यावरणीय, सामाजिक व प्रशासनिक चुनौतियाँ, सरकारी प्रयास व नीतियाँ, तथा संभावित समाधान एवं नीति-सिफारिशों पर विस्तृत चर्चा करेंगे।
भारत में रामसर स्थलों की राज्यवार सूची (2025 तक)
भारत के रामसर स्थलों का विस्तार देश के अधिकांश भौगोलिक क्षेत्रों में हो चुका है। निम्न तालिका में जून 2025 तक के राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अनुसार सभी 91 रामसर स्थलों की सूची और संख्या प्रदर्शित है :
• आंध्र प्रदेश (1): कोल्लेरू झील (Kolleru Lake)
• असम (1): दीपोर बील (Deepor Beel)
• बिहार (3): कबरताल झील (काँवर ताल या कांवर झील), नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य
• गोवा (1): नंदा झील (Nanda Lake)
• गुजरात (4): खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, नलसरोवर पक्षी अभयारण्य, ठोल झील, वधावन आर्द्रभूमि
• हरियाणा (2): सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य
• हिमाचल प्रदेश (3): चंद्रताल, पौंग बांध झील (महाराणा प्रताप सागर) वन्यजीव अभयारण्य, रेणुका झील
• जम्मू एवं कश्मीर (5): होकरसर आर्द्रभूमि, हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिज़र्व, शालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिज़र्व, सुरिनसर-मंसार वन्यजीव अभयारण्य, वुलर झील
• झारखंड (1): उधवा झील पक्षी अभयारण्य
• कर्नाटक (4): रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, अनकासमुंद्रा पक्षी संरक्षित क्षेत्र, अग्नाशिनी эстुअरी (नदी मुहाना), मागडी केरे संरक्षण रिज़र्व
• केरल (3): अष्टमुडी झील, सप्तकोट्टा झील (सास्तमकोट्टा), वेम्बनाड-कोल आर्द्रभूमि
• लद्दाख (2): त्सो कर झील, त्सो मोरीरी झील
• मध्य प्रदेश (5): भोज वेटलैंड (भोपाल की बड़ी एवं छोटी झीलें), सखिया सागर, सिरपुर झील, यशवंत सागर, तवा जलाशय
• महाराष्ट्र (3): लोनार झील, नंदूर मधमेश्वर, ठाणे क्रीक आर्द्रभूमि
• मणिपुर (1): लोकटक झील
• मिज़ोरम (1): पालक झील (पाला आर्द्रभूमि)
• ओडिशा (6): अंसुपा झील, भितरकनिका मैंग्रोव, चिलिका झील, हीराकुद जलाशय, सतकोसिया घाटी, ताम्परा झील
पंजाब (6): बियास संरक्षण रिज़र्व, हरिके झील, कंजली झील, केशोपुर-मींझा समुदाय रिज़र्व, नंगल वन्यजीव अभयारण्य, रोपड़ (रूपनगर) झील
• राजस्थान (4): केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सांभर झील, खीचन आर्द्रभूमि, मेनार आर्द्रभूमि
• सिक्किम (1): खेचेओपलरी झील (पवित्र खेचुपेरी झील)
• तमिलनाडु (20): चितरंगुडी पक्षी अभयारण्य, कांजीरंकुलम पक्षी अभयारण्य, कराइवेट्टी पक्षी अभयारण्य, करिकिली पक्षी अभयारण्य, कुन्ठनकुलम पक्षी अभयारण्य, कोडीकराई (प्वाइंट कैलिमेरे) वन्यजीव एवं पक्षी अभयारण्य, लंबी शोला (लॉन्गवुड शोला) रिज़र्व फ़ॉरेस्ट, पल्लिकरणई मार्श रिज़र्व फ़ॉरेस्ट, पिचावरम मैंग्रोव वन, विच्छितवाडु (उदयमार्तंडपुरम) पक्षी अभयारण्य, वडवर पक्षी अभयारण्य, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य, वेल्लोड पक्षी अभयारण्य, वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि комплекс, नांजरायन पक्षी अभयारण्य, कज़ुवेली आर्द्रभूमि, सक्कराकोट्टई पक्षी अभयारण्य, तेरठंगल पक्षी अभयारण्य, सुचिन्द्रम थेरूर आर्द्रभूमि संकुल, कठीपारा कुंडार (सूचीबद्ध नाम) – (तमिलनाडु में स्थल संख्या देश में सर्वाधिक है)
• त्रिपुरा (1): रुद्रसागर झील
• उत्तर प्रदेश (10): बाखीरा पक्षी विहार, हैदरपुर आर्द्रभूमि, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती आर्गा पक्षी अभयारण्य, सामन पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, संडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नवर झील, सुर सरोवर झील, Upper Ganga नदी आर्द्रभूमि (ब्रजघाट से नरौरा तक)
• उत्तराखंड (1): आसन बेराज आर्द्रभूमि
• पश्चिम बंगाल (2): पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, सुंदरबन आर्द्रभूमि (भारतीय हिस्सा)
उपरोक्त सूची से स्पष्ट है कि भारत में रामसर स्थलों का वितरण भौगोलिक रूप से विस्तृत है। तमिलनाडु (20 स्थल), उत्तर प्रदेश (10 स्थल), पंजाब (6 स्थल) तथा ओडिशा (6 स्थल) जैसे राज्यों में इनकी संख्या अधिक है , जबकि सिक्किम, झारखंड, गोवा आदि ने हाल ही में अपना पहला रामसर स्थल प्राप्त किया है । कई स्थल अंतरराज्यीय नदी-घाटियों या तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, जो पारिस्थितिकीय रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। राज्यवार सूची बनने से नीति-निर्माताओं को क्षेत्रीय स्तर पर संरक्षण प्रयास केंद्रित करने में सुविधा मिलती है।
2022-2025 के दौरान जुड़े नए रामसर स्थलों पर विशेष फोकस
पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने कई प्रमुख जलक्षेत्रों को रामसर सूची में शामिल करवाने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। 2022 से 2025 के बीच भारत में दर्जनों नए रामसर स्थल जोड़े गए, जिससे कुल संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है । यह दौर भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ (साल 2022) से आरंभ होकर अब तक जारी है, जिसमें सरकार ने “75वें स्वतंत्रता वर्ष में 75 रामसर स्थल” का लक्ष्य भी पूर्ण किया । वर्ष 2022 की शुरुआत में भारत में लगभग 49 रामसर स्थल थे, लेकिन उसी वर्ष विभिन्न चरणों में करीब 26 नए स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की सूची में सम्मिलित किया गया। उदाहरणस्वरूप, फरवरी 2022 में दो नये रामसर स्थल (खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, गुजरात एवं भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा) जोड़े गए, अप्रैल 2022 में तमिलनाडु के कई छोटे पक्षी अभयारण्य (जैसे करिकिली, पल्लिकरणई मार्श, पिचावरम मैंग्रोव, आदि) रामसर सूची का हिस्सा बने , जबकि अगस्त 2022 तक भारत कुल 75 रामसर स्थलों का आकड़ा छू चुका था। 2022 में शामिल अन्य प्रमुख स्थलों में साख्या सागर (माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश), सिरपुर झील (इंदौर, म.प्र.), ठाणे क्रीक (महाराष्ट्र), सुचिन्द्रम-थेअरूर आर्द्रभूमि परिसर (तमिलनाडु), होकर्सर, शालबुग व हाइगम वेटलैंड्स (कश्मीर) आदि शामिल हैं। 2022 की उल्लेखनीय बात यह रही कि दक्षिण भारत (विशेषकर तमिलनाडु) के कई लघु पक्षी अभयारण्यों को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली।
साल 2023 में भी यह रुझान जारी रहा, हालाँकि गति थोड़ी धीमी थी। फरवरी 2023 में कर्नाटक के तीन महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थलों – अनकासमुंद्रा, अग्नाशिनी एस्टुअरी (नदीमुख) तथा मागडी केरे – को रामसर टैग प्रदान किया गया। इसी प्रकार मई 2023 में तमिलनाडु के दो स्थल – कराइवेट्टी पक्षी अभयारण्य तथा लॉन्गवुड शोलार रिज़र्व फ़ॉरेस्ट – सूचीबद्ध हुए। वर्ष के उत्तरार्ध में, अक्टूबर 2023 में बिहार के नागी एवं नकटी पक्षी अभयारण्य (जमुई जिला) को रामसर सूची में शामिल किया गया । इन दोनों कृत्रिम जलाशयों का जोड़ना विशेष महत्त्वपूर्ण था क्योंकि इससे पूर्व बिहार जैसे राज्यों का रामसर सूची में प्रतिनिधित्व बेहद कम था। नागी-नकटी की जोड़ से भारत ने 82 रामसर स्थलों का आंकड़ा छूकर चीन की बराबरी कर ली थी (चीन के भी 82 रामसर स्थल थे) और एशिया में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर था ।
वर्ष 2024 की शुरुआत में ही कुछ अहम घोषणाएँ हुईं। जनवरी 2024 में मध्य प्रदेश के बड़े तवाReservoir (तवा बाँध जलाशय) को रामसर स्थल घोषित किया गया । साथ ही, तमिलनाडु के नांजरायण पक्षी अभयारण्य और कज़ुवेली आर्द्रभूमि (दोनों जनवरी 2024 में) रामसर सूची में आए, जिससे तमिलनाडु के स्थलों की संख्या 18 से बढ़कर 20 होने के करीब पहुँची । फरवरी 2024 तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 85 तक पहुँच गई थी । उल्लेखनीय है कि 2024 में जोड़े गए अधिकांश स्थल छोटे या मध्यम आकार के थे, परंतु ये स्थानीय स्तर पर पारिस्थितिकी संतुलन हेतु अति महत्त्वपूर्ण हैं।
वर्ष 2025 की बात करें तो 2 फरवरी 2025 (विश्व आर्द्रभूमि दिवस) पर भारत ने एक साथ चार नए रामसर स्थलों की घोषणा की – तमिलनाडु के सक्कराकोट्टई पक्षी अभयारण्य और तेरठangal पक्षी अभयारण्य, सिक्किम की पवित्र खेचेओपलरी झील और झारखंड की उधवा झील (पक्षी अभयारण्य) । इन घोषणाओं की दो विशिष्ट उपलब्धियाँ रहीं: सिक्किम एवं झारखंड जैसे प्रदेशों को उनका पहला रामसर स्थल प्राप्त हुआ, तथा तमिलनाडु में कुल स्थलों की संख्या बढ़कर देश में सर्वाधिक 20 हो गई । अंतत: जून 2025 में राजस्थान के दो प्रसिद्ध आर्द्रभूमि स्थलों – खीचन (फलोदी) की झीलें, जो सर्दियों में डेमोइसेल क्रेन्स (कुरजां) के लिए प्रसिद्ध हैं, तथा मेّنार (उदयपुर) की झीलें, जो ग्रेटर फ़्लेमिंगो एवं मोर समेत सैकड़ों प्रजातियों का आश्रय हैं – को रामसर मान्यता मिली । इन जुड़ावों के साथ भारत के रामसर स्थलों की कुल संख्या 91 तक पहुंच गई । नए स्थलों के जुड़ने से संबंधित राज्यों में उत्साह है – उदाहरणस्वरूप, राजस्थान में खीचन व मेनार को रामसर टैग मिलने पर इन्हें विश्व स्तर पर पर्यटन व पक्षी-अध्ययन के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजनाएँ बनी हैं । सारांशतः, 2022-25 के दौरान जोड़े गए अधिकतर रामसर स्थल या तो पहली बार उपेक्षित रहे क्षेत्रों से हैं (जैसे तमिलनाडु के छोटे पक्षी अभयारण्य, बिहार के मानव-निर्मित जलाशय) या महत्त्वपूर्ण प्रवासी पक्षी आश्रय क्षेत्र हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में जुड़ना भारत के जैव-विविधता संरक्षण प्रयासों को वैश्विक मंच देता है।
रामसर स्थलों के समक्ष पर्यावरणीय, सामाजिक एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ
हालाँकि रामसर सूची में शामिल होकर कोई आर्द्रभूमि अंतरराष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त कर लेती है और सरकार की प्रतिबद्धता बढ़ जाती है, किंतु स्थल स्तर पर कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भारत के अधिकांश रामसर स्थल विविध प्रकार के दबावों का सामना कर रहे हैं – चाहे वे पर्यावरणीय हों, स्थानीय सामाजिक-आर्थिक कारक हों या प्रशासनिक व नीति-क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दे। नीचे इन चुनौतियों का वर्गीकरण सहित वर्णन किया गया है:
पर्यावरणीय चुनौतियाँ
पर्यावरणीय दृष्टि से भारत की आर्द्रभूमियाँ अनेक समस्याओं से जूझ रही हैं। WWF-इंडिया के अनुसार भारत में आर्द्रभूमियाँ सबसे तेज़ी से नष्ट हो रहे पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं । वनस्पति ह्रास, मृदा एवं गाद जमाव (siltation), लवणीकरण (salinization), मौसम के पैटर्न में परिवर्तन से होने वाली अत्यधिक बाढ़ या सूखे की स्थितियाँ, बढ़ते प्रदूषण (नगरीय सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट का प्रवाह), तथा आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रसार – ये सभी मिलकर wetlands के स्वास्थ्य को क्षति पहुँचा रहे हैं । कई रामसर स्थलों में जल-स्तर का मौसमी असंतुलन देखने को मिलता है; उदाहरणतः कश्मीर की आर्द्रभूमियाँ (होकरसर, हाइगम, आदि) कभी पानी की कमी तो कभी बाढ़ से प्रभावित होती हैं, जिससे प्रवासी पक्षियों का आगमन घटने लगा था। विशेषज्ञ बताते हैं कि यदि इन जलाशयों में पर्याप्त एवं समय पर जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तो ये फिर से लाखों पक्षियों को आश्रय दे सकते हैं । इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन लंबे समय में आर्द्रभूमियों के भू-जल भराव, प्रवासी पक्षियों के मार्ग, तथा मैंग्रोव जैसे तटीय वेटलैंड पर गहरा प्रभाव डाल रहा है – समुद्र स्तर वृद्धि सुंदरबन जैसे रामसर स्थलों के अस्तित्व के लिए ख़तरा बन रही है, वहीं हिमालयी उच्च हिमझीलों के लिए ग्लेशियर पिघलना व मौसम अनिश्चितता नई चुनौती है।
कई आर्द्रभूमियों का जलीय पारिस्थितिकी संतुलन भी मानवजनित कारणों से बिगड़ा है। उदाहरण के लिए, पंजाब एवं हरियाणा की रामसर सूचीबद्ध झीलों (हरिके, सतलुज-बियास आदि) में अपस्ट्रीम बाँधों व नहरों के कारण जल के आवर्तन (flushing) में कमी आई है। उत्तर प्रदेश की कुछ झीलें सिंचाई के लिए अत्यधिक पानी निकाले जाने से सूखाव का शिकार होती हैं। कई स्थल प्रदूषण के भार से दबे हैं – जैसे पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि को कोलकाता महानगर का अपशिष्ट जल ढोना पड़ता है, दीपोर बील (गुवाहाटी) शहर का कूड़ा-कचरा डंपिंग ग्राउंड बन चुका है , दिल्ली से सटा सुर सरोवर (कीथम झील) भी सीवेज और कचरे की मार झेल रहा है। विषैले रासायनिक प्रदूषकों के अंश जलचरों व पक्षियों की खाद्य शृंखला में प्रवेश कर रहे हैं जिससे जैव-विविधता को दीर्घकालीन क्षति होती है। कई वेटलैंड में तेजी से फैलती जलकुंभी (Water Hyacinth) जैसी विदेशी प्रजातियाँ जल के खुले क्षेत्र को ढक कर उसका ऑक्सीजन संतुलन बिगाड़ देती हैं, जैसा कि लोकटक झील (मणिपुर) व कबरताल (बिहार) में देखा गया है।
आवास (habitat) क्षरण भी एक बड़ी समस्या है। नगरों के पास की आर्द्रभूमियाँ लगातार घटती आकार की हैं – WWF की रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ दशकों में मुंबई ने 71% वेटलैंड खो दिए, चेन्नई ने 85% और कोलकाता ने 36% आर्द्रभूमि क्षेत्र खो दिया है । wetlands को अक्सर “बेकार पड़ती ज़मीन” समझ कर भर कर उस पर निर्माण कार्य कर दिया जाता है । इसके उदाहरण हर शहर में मिलेंगे – बेंगलुरु की झीलों पर रियल एस्टेट कॉलोनियाँ बन गईं, श्रीनगर में डल झील जैसे जलाशयों को भरकर निवास बनाए गए, यहाँ तक कि छोटे ग्रामीण तालाबों और दलदलों को भी खेत या आवास भूमि में बदलने की प्रवृत्ति आम है। तटीय क्षेत्रों में भी मैंग्रोव व दलदली पारिस्थितिकी को साफ कर मत्स्य पालन, झींगा खेती या पर्यटन ढाँचों के लिए भूमि निकाली जा रही है, जिससे तटीय रामसर साइट (जैसे भितरकनिका, सुंदरबन) के बफर क्षेत्र कम हो रहे हैं। इन सभी मानवजनित गतिविधियों का नतीजा यह है कि कई रामसर स्थलों की पर्यावरणीय गुणवत्ता गिर रही है और उनमें पाए जाने वाले कई दुर्लभ पक्षी-पशु संकट में हैं।
यहाँ ध्यान देने योग्य है कि रामसर कन्वेंशन के तहत बनाए गए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दुनिया भर के वे रामसर स्थल सूचीबद्ध होते हैं जिनका पारिस्थितिक चरित्र मानवीय हस्तक्षेप या अन्य कारणों से क्षरित हो रहा है । भारत के दो रामसर स्थल – केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) एवं लोकटक झील (मणिपुर) – वर्तमान में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज हैं क्योंकि ये स्थल जल अभाव, प्रदूषण और invasive प्रजातियों जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रभाव कितने गंभीर हो सकते हैं यदि समय रहते कदम न उठाए जाएँ।
सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियाँ
आर्द्रभूमियाँ सिर्फ पारिस्थितिक मूल्य ही नहीं रखतीं, वे लाखों लोगों की आजीविका और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ी हैं। भारत के अधिकतर रामसर स्थलों के आसपास स्थानीय समुदाय सदियों से मत्स्य पालन, कृषि, सिंचाई, घास-फलस संग्रह, नाव परिवहन एवं आजीविका के अन्य कार्यों पर निर्भर रहे हैं। ऐसे में इन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के बाद स्थानीय समुदायों के हितों को संतुलित करना एक चुनौती बन जाता है। कई जगह संरक्षण उपायों के तहत मछली पकड़ने, चारा कटाई, शिकार आदि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष पनप सकता है। उदाहरणतः, लोकटक झील में संरक्षित क्षेत्र घोषित होने के बाद पारंपरिक मत्स्य कृषकों और वन विभाग के बीच विवाद उभरे; कोलेरू झील (आंध्र प्रदेश) के आसपास मछुआरे तथा कृषक वर्ग रामसर टैग से आशंकित रहते हैं कि कहीं उनके उपयोग के अधिकार सीमित न हो जाएँ।
जनभागीदारी की कमी भी एक सामाजिक चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि रामसर मान्यता के लिए साइट चयन एवं प्रबंधन योजनाओं में ज़मीनी स्तर पर समुदायों की पर्याप्त सहभागिता नहीं होती। South Asia Network for Dams, Rivers and People (SANDRP) द्वारा किए गए आकलन में पाया गया कि रामसर सूची में शामिल करने की प्रक्रिया में प्राथमिक हितधारकों और स्थानीय नागरिकों से परामर्श अपेक्षाकृत कम होता है । नतीजतन, स्थानीय लोगों को अक्सर इस टैग के मायने, लाभ और दायित्वों की जानकारी नहीं होती। जागरूकता का अभाव एक बड़ी समस्या है – ग्रामीण इलाकों में कई लोग रामसर सम्मेलन के बारे में नहीं जानते, न ही यह समझते हैं कि उनकी अपनी आर्द्रभूमि वैश्विक महत्त्व की है। इस कारण कई स्थानों पर लोग अनजाने में अवैधानिक गतिविधियाँ (जैसे शिकार, पेड़ कटाई, कचरा फेंकना) जारी रखते हैं जो साइट की सेहत के लिए हानिकारक हैं।
आर्द्रभूमियों का एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू उनका पर्यटन एवं सौंदर्यीकरण है। पक्षी-दर्शन और प्रकृति-पर्यटन आज कई रामसर स्थलों पर बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिल सकता है। किंतु अगर इसे सही तरीके से प्रबंधित न किया जाए तो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। अतिरिक्त पर्यटन दबाव से प्रदूषण, शोर, तथा वन्यजीवों को तनाव होने की आशंका रहती है। कुछ जगहों पर सरकारों ने रामसर स्थलों पर पर्यटक सुविधाओं के नाम पर भारी निर्माण कार्य करवा दिए – जैसे पक्के रास्ते, व्यूइंग टॉवर, नाव जेट्टी, गेस्ट हाउस आदि। पर्यावरणविद् डॉ. असद रह़मानी जैसे विशेषज्ञ कहते हैं “किसी भी आर्द्रभूमि को कृत्रिम तरीके से ‘सुंदर’ बनाने की ज़रूरत नहीं; प्रकृति अपने मूल रूप में ही सुंदर है। भारी सीमेंटेड निर्माण और सौंदर्यीकरण की परियोजनाएँ wetlands को नुकसान पहुँचा सकती हैं” । उदाहरण के लिए, भोपाल की भोज वेटलैंड (ऊपरी एवं निचली झील) के चारों ओर बड़े पैमाने पर लेक-व्यू उद्यान और सड़कें बन जाने से प्राकृतिक दलदली किनारे घट गए और अब यह रामसर साइट प्रदूषण व अतिक्रमण के चलते ख़तरे में है । पर्यटन बढ़ने से कुछ स्थानों पर अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या भी आई है – पर्यटक प्लास्टिक, पैकेजिंग आदि कचरा छोड़ जाते हैं जो झीलों में जमा होता है।
सामाजिक चुनौतियों का एक और आयाम मानव-वन्यजीव द्वंद्व है। कई wetlands, विशेषकर जो राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य हैं, वहाँ पक्षियों या जीवों द्वारा पास के खेतों में नुकसान पहुँचाने की घटनाएँ होती हैं (जैसे पक्षी धान की फसल खा जाते हैं, या जलसूअर मक्का आदि रौंद देते हैं)। इससे स्थानीय किसान कभी-कभी आक्रोश में आकर उन जीवों को मारने या भगाने के तरीके अपनाते हैं। यह प्रवृत्ति रामसर स्थलों में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को कमजोर करती है। अतः, समुदायों को साथ लेकर चलना तथा उनके आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए संरक्षण करना एक बड़ी चुनौती है।
प्रशासनिक एवं शासन संबंधी चुनौतियाँ
भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए कानूनी-प्रशासनिक ढाँचा मौजूद तो है, किंतु धरातल पर क्रियान्वयन में कई कमियाँ देखने को मिलती हैं। पहली बात, देश में 2 लाख से अधिक आर्द्रभूमियाँ हैं, परंतु केवल 102 के करीब wetlands को ही सरकार ने आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया है । अधिकांश राज्यों में अभी सैकड़ों छोटे-बड़े wetlands ऐसी स्थिति में हैं जिनकी सीमा, महत्व आदि का कोई प्रावधानिक रिकॉर्ड नहीं। 2017 में पर्यावरण मंत्रालय ने आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 अधिसूचित किए, जिनके तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण बनाना तथा महत्त्वपूर्ण wetlands की सूची अधिसूचित करना अनिवार्य है । लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई राज्यों ने इन प्राधिकरणों को महज कागज़ी संस्था बनाकर छोड़ा हुआ है; कुछ राज्यों में ये नियमित बैठक तक नहीं करते । विशेषज्ञ कहते हैं कि “कई बार इन प्राधिकरणों के अधिकारियों को स्वस्थ आर्द्रभूमि के कार्यकरण की बुनियादी जानकारी भी नहीं होती” । केंद्र एवं राज्य सरकारों ने wetlands संरक्षण हेतु अनेक नीतियाँ एवं कानून बनाए हैं, परंतु कमजोर प्रवर्तन (weak enforcement) के चलते उनका प्रभाव सीमित रहा है ।
पर्याप्त संसाधनों की कमी भी बड़ी चुनौती है। आर्द्रभूमियों के प्रबंधन के लिए विशेष बजट, कर्मियों का प्रशिक्षण, वैज्ञानिक अध्ययन आदि की जरूरत होती है। वर्तमान में अधिकांश रामसर स्थलों का प्रबंधन संबंधित राज्य के वन विभाग या मत्स्य विभाग के हाथ में है, जिनके पास सीमित बजट एवं जनशक्ति है। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (NWCP) और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (NLCP) जैसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 2013 में मिलाकर राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (NPCA) तो बनाई गई , लेकिन राज्यों से प्रस्ताव आने, धन आबंटन और उसके उपयोग की प्रक्रिया सुस्त रहती है। प्रभावी मॉनिटरिंग तंत्र का अभाव एक गंभीर मुद्दा है – अधिकतर रामसर स्थलों के लिए प्रबंधन योजना तो कागज़ पर है, परंतु उसकी प्रगति को मापने के लिए कोई केंद्रीकृत निगरानी नहीं। SANDRP की रिपोर्ट के अनुसार “सरकार ने इन स्थलों के खतरों का आकलन कर उनका समाधान निकालने हेतु कोई ठोस कार्ययोजना तैयार नहीं की, न ही विश्वसनीय निगरानी तंत्र विकसित किया है” । परिणामस्वरूप, कई रामसर साइट्स में स्थिति बिगड़ती रही पर समय पर चेतावनी नहीं ली गई।
अंतर-विभागीय समन्वय की कमी भी शासन पक्ष की बड़ी चुनौती है। आर्द्रभूमियों का सरोकार केवल वन या पर्यावरण विभाग से नहीं, बल्कि सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग, मत्स्य पालन, कृषि, पर्यटन आदि अनेक शाखाओं से है। व्यवहार में देखने में आता है कि इन विभागों के बीच तालमेल का अभाव wetlands को नुकसान पहुँचा रहा है – उदाहरणतः एक विभाग तालाब गहरीकरण का ठेका देता है तो दूसरा विभाग उसी तालाब में पार्क बनाने लगता है बिना पारिस्थितिक असर का मूल्यांकन किए। कई शहरी आर्द्रभूमियाँ नगर निगम, विकास प्राधिकरण और वन विभाग के बीच अधिकार क्षेत्र के विवाद में उलझी रहती हैं कि उसका मालिकाना किसके पास हो, जिससे कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता और अतिक्रमण होते जाते हैं। नीति-स्तर पर स्पष्टता की कमी भी कही जा सकती है – 2017 के नए नियमों में कई गतिविधियों (जैसे कृषि, ज़ोन निर्धारण) को राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया, जिससे कुछ विवाद उपजे कि क्या संरक्षित हो और क्या नहीं। कुछ विश्लेषकों ने 2017 के नियमों की यह कहकर आलोचना की कि इससे पहले मौजूद केंद्रीय निगरानी ढांचा हटा दिया गया और आर्द्रभूमि की परिभाषा से ऐसी कई श्रेणियाँ निकाल दी गईं जिन्हें संरक्षण मिलना चाहिए था ।
इन प्रशासनिक कमियों का प्रभाव यह हुआ है कि रामसर टैग मिलने के बाद भी कई स्थलों की स्थिति में ज़मीनी सुधार नहीं दिखता। उदाहरण के लिए, कश्मीर की वूलर झील 1990 में रामसर सूची में आई, मगर आज भी वह अतिक्रमण और गाद जमाव से जूझ रही है; भोपाल की भोज झीलें 2002 में सूचीबद्ध हुईं पर बढ़ते शहरी दबाव ने उन्हें मॉनिटरिंग के अभाव में ख़राब कर दिया है; सांभर झील (राजस्थान) तो रामसर साइट होने के बावजूद हाल ही में हजारों पक्षियों की रहस्यमयी मौत (ऐवियन बोटुलिज़्म) के लिए खबरों में आई, जिससे यह सवाल खड़े हुए कि क्या सिर्फ अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलना पर्याप्त है? स्पष्ट है कि चुनौतियाँ बहु-आयामी हैं और उनसे निपटने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण की ज़रूरत है, जिसकी चर्चा हम अगले खंड में करेंगे।
संरक्षण हेतु सरकारी प्रयास, योजनाएँ एवं नीतियाँ
आर्द्रभूमि संरक्षण की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं। इन प्रयासों को कानूनी रूपरेखा, नीतिगत योजना, वित्तीय पहल व जागरूकता कार्यक्रमों के तौर पर देखा जा सकता है। नीचे मुख्य सरकारी पहलों और नीतियों का सार प्रस्तुत है:
• कानूनी एवं संस्थागत ढाँचा: आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु सबसे पहला व्यापक कदम 2010 में आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमावली, 2010 को लागू करना था, जिसे बाद में अद्यतन कर आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 बनाया गया। 2017 के नियमों के तहत राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति (National Wetlands Committee) का गठन हुआ और प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण बनाने का प्रावधान किया गया । राज्य प्राधिकरण की अध्यक्षता संबंधित प्रदेश के पर्यावरण मंत्री करते हैं। इन नियमों ने राज्यों को अधिकार दिया कि वे अपने यहाँ महत्वपूर्ण wetlands चिन्हित कर राजपत्रित अधिसूचना द्वारा संरक्षित करें, साथ ही प्रत्येक अधिसूचित आर्द्रभूमि के लिए विस्तृत प्रबंधन योजना बनाएँ। नियमों में आर्द्रभूमियों में कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध का प्रावधान है (जैसे ठोस अपशिष्ट डालना, स्थायी निर्माण, अतिक्रमण) तथा कुछ को नियंत्रणाधीन अनुमति की श्रेणी में रखा गया है। इन नियमों की एक कमी यह है कि इनकी परिभाषा में नदियों की मुख्य धारा, धान के खेत आदि को आर्द्रभूमि से बाहर रखा गया है , जिसके लिए आलोचना भी हुई क्योंकि कई नदी-तटवर्ती क्षेत्र आर्द्रभूमि जैसे ही पारिस्थितिक लाभ देते हैं। फिर भी, 2017 के नियम मौजूदा ढाँचे को सशक्त करने की दिशा में एक कदम हैं।
राष्ट्रीय योजनाएँ एवं वित्त: भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (NWCP) 1985 में, तथा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (NLCP) 2001 में शुरू की थी। 2013 में इन दोनों को मिलाकर राष्ट्रीय जलीय पारितंत्र संरक्षण योजना (NPCA) बनाई गई । NPCA के तहत केंद्र सरकार राज्यों की प्रस्तावित आर्द्रभूमि/झील परियोजनाओं को वित्तपोषित करती है। 2014 के बाद रामसर साइट्स की संख्या बढ़ने पर केंद्र ने बजट आवंटन बढ़ाया है, लेकिन फंडिंग अभी भी चुनिंदा बड़ी झीलों/तालाबों तक सीमित है। 2023-24 के केंद्रीय बजट में पहली बार “आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु अमृत धरोहर योजना” की घोषणा की गई । इस अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य अगले तीन वर्षों में देश की आर्द्रभूमियों का संतुलित एवं टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करना है, जिसमें जैव-विविधता बढ़ाना, कार्बन भंडारण क्षमता बढ़ाना, ईको-टूरिज़्म को प्रोत्साहन और स्थानीय आजीविका सुधार जैसे घटक शामिल हैं । अमृत धरोहर के तहत कुछ चुनींदा रामसर स्थलों को पायलट स्तर पर विकास का मॉडल बनाने की योजना है।
• विशिष्ट कार्यक्रम एवं अभियान: 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार ने प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों के संरक्षण-पुनर्जीवन का लक्ष्य रखकर “अमृत सरोवर” अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत कुछ रामसर स्थलों को भी चुना गया और धनराशि आवंटित हुई। हालांकि, विशेषज्ञों ने पाया कि कई जगह इस फंड का उपयोग आर्द्रभूमि के भीतर गैर-ज़रूरी कंक्रीट निर्माण पर हुआ जो मूल उद्देश्य के विपरीत था । फिर भी, इसने ज़िला स्तर पर wetlands की पहचान और उन पर कार्यवाही का सिलसिला शुरू किया। MoEF&CC (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) ने 2020 में एक “Wetlands Rejuvenation Programme” चलाया, जिसके तहत 500 से अधिक आर्द्रभूमियों का आधारभूत डाटाबेस तैयार करना, त्वरित आकलन (rapid assessment), हितधारक परामर्श तथा प्रबंधन योजनाएँ बनाना शामिल था । इसी तरह, नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 2021 से गंगा नदी बेसिन के आसपास 500+ wetlands के “हेल्थ-कार्ड” बनाए जाने व उनकी بحाली की योजनाएँ तैयार करने का काम शुरू हुआ । राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-2031) में भी wetlands को एक अलग से ध्यान देने योग्य विषय बनाया गया है और एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि मिशन स्थापित करने की संस्तुति की गई है ।
• क्षेत्र-विशेष संरक्षण प्रयास: कुछ आर्द्रभूमियों के लिए केंद्र/राज्य सरकारों ने विशेष प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण गठित किए हैं। जैसे चिलिका झील, ओडिशा के लिए चिलिका विकास प्राधिकरण 1991 में बना जिसने झील के पारिस्थितिक पुनर्जीवन में सफलता पाई (2002 में चिलिका झील को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया था)। लोकटक झील, मणिपुर के लिए लोकटक विकास प्राधिकरण सक्रिय है। कई रामसर साइट्स जैसे वुलर झील, सांभर झील, etc. के लिए राज्य सरकारों ने अलग से कार्ययोजनाएँ बनाईं हैं। तटीय आर्द्रभूमियों की रक्षा हेतु तटीय क्षेत्र विनियमन (CRZ) अधिसूचना 2011 और 2019 में लाई गई, जिसके तहत समुद्री तटों, खाड़ियों, मैंग्रोव व दलदलों को संरक्षित क्षेत्रों की श्रेणियों में रखा गया है । इसके अलावा केंद्र ने wetlands को आपदाओं से बचाने हेतु NDMA के जरिए गाइडलाइन्स जारी की हैं, तथा कुछ स्थलों के लिए विदेशों के साथ मिलकर “Twinning” कार्यक्रम (जुड़वाँ साइट साझेदारी) भी किये गए हैं।
• शोध, शिक्षा एवं जागरूकता: सरकार विज्ञान एवं तकनीक का उपयोग कर आर्द्रभूमि निगरानी को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। इसरो के सहयोग से राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दशकीय परिवर्तन एटलस तैयार किया गया है जिसमें पिछले 10 वर्षों में देश के wetlands क्षेत्र में आए बदलावों की सैटेलाइट सूचना संकलित है । कई रामसर साइट्स (जैसे चिलिका झील) में अब रिमोट सेंसिंग एवं ड्रोन तकनीक से जल गुणवत्ता, जल स्तर व वनस्पति कवर की निगरानी की जाती है । पर्यावरण मंत्रालय की ओर से एक समर्पित पोर्टल indianwetlands.in लॉन्च किया गया है जिसमें सभी रामसर स्थलों की इंटरैक्टिव मैप एवं राज्यवार सूची उपलब्ध है । हर साल 2 फ़रवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम, स्कूल-कॉलेज प्रतियोगिताएँ, प्रकाशन आदि आयोजित किए जाते हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी देश में क्षेत्रीय रामसर केंद्रों से अधिकारी प्रशिक्षण लेते हैं। इन सब प्रयासों का उद्देश्य आर्द्रभूमि संरक्षण को मुख्यधारा (mainstream) में लाना है ।
इन सरकारी कदमों के चलते कई स्थानों पर सुधार के संकेत भी दिखाई दिए हैं। उदाहरण के लिए, नंदूर मधमेश्वर (महाराष्ट्र) में रामसर टैग के बाद अवैध शिकार पर लगभग पूर्ण विराम लगा है और पक्षियों की संख्या बढ़ी है; भिंडावास (हरियाणा) में प्रदूषण स्रोतों को चिन्हित कर कार्यवाही की गई है; सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आसपास के ज़मीन अधिग्रहण कर आर्द्रभूमि विस्तार किया जा रहा है; कूबरताल, बिहार में मछुआरों को वैकल्पिक आजीविका प्रशिक्षण दिए गए हैं। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जब नीतियाँ सही ढंग से लागू की जाती हैं, तो रामसर स्थलों को दी गई अंतरराष्ट्रीय पहचान संरक्षण के ठोस कार्यों में परिवर्तित हो सकती है।
संभावित समाधान और नीति सिफारिशें
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सिर्फ सूची में नाम दर्ज होना पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रत्येक रामसर स्थल के दीर्घकालीन संरक्षण एवं “समझदारी भरे उपयोग” (wise use) के लिए बहु-आयामी रणनीति अपनानी होगी। निम्नलिखित कुछ समाधान एवं नीतिगत सिफारिशें हैं, जो विशेषज्ञों और विभिन्न रिपोर्टों द्वारा सुझाई गई हैं:
- समग्र पारिस्थितिकी दृष्टिकोण एवं कैचमेंट प्रोटेक्शन: आर्द्रभूमि को उसके जलागम (कैचमेंट) क्षेत्र समेत एक इकाई मानकर प्रबंधन करना जरूरी है। Ramsar COP14 (2022) ने ज़ोर दिया कि wetlands को बड़े परिदृश्य (लैंडस्केप) के संदर्भ में बचाया जाए । इसके लिए आवश्यक है कि प्राकृतिक जल प्रवाह को बनाए रखा जाए, आर्द्रभूमि को पोषित करने वाली नदियों-जलधाराओं पर अनियोजित बाँध या परिवर्तन न हों, और अपस्ट्रीम क्षेत्रों में वनों का संरक्षण हो। प्रत्येक रामसर स्थल के लिये कैचमेंट एरिया को अधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज कर उसे भी अवैध खनन, कटाव से बचाने की सिफारिश की जाती है । उदाहरण के तौर पर, भूटान के साथ मिलकर असम की मानस आर्द्रभूमि का पारिस्थितिकी प्रवाह बनाए रखने हेतु समझौते किये जा सकते हैं; बेंगलुरु की लुप्तप्राय झीलों को उनके अधिकतम फैलाव स्तर पर सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना चाहिए । कैचमेंट सुरक्षा के बिना wetlands टापू की तरह जीवित नहीं रह सकते।
- कड़े प्रवर्तन एवं मॉनिटरिंग: मौजूदा कानूनों-नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। हर रामसर स्थल के लिए एक नोडल प्रबंधन एजेंसी तय कर उसके माध्यम से नियमित निगरानी (monitoring) होनी चाहिए। आधुनिक तकनीकों जैसे उपग्रह चित्रण, जीआईएस आधारित ट्रैकिंग से जल स्तर, भूमि उपयोग परिवर्तन, प्रदूषण स्रोत आदि पर नजर रखी जानी चाहिए । सरकार एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि स्वास्थ्य कार्ड प्रणाली विकसित कर सकती है, जिसमें प्रत्येक साइट के मुख्य पैरामीटर (जैसे जल की गुणवत्ता, प्रवासी पक्षियों की संख्या, मैक्रोफाइट कवर, आदि) को ग्रेडिंग दी जाए। यदि कोई साइट लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है तो सतर्कता (अलर्ट) जारी कर केंद्रीय हस्तक्षेप किया जाए। साथ ही, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों की नियमित बैठकें, क्षमतावर्धन (capacity building) प्रशिक्षण आयोजित हों ताकि वे अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह रहें। आवश्यकता पड़ने पर 2017 के नियमों की समीक्षा कर केंद्रीय निगरानी को और मजबूत करने हेतु संशोधन किया जाना चाहिए ।
- स्थानीय समुदायों की भागीदारी एवं सह-विकास: “संरक्षण व आजीविका” को साथ लेकर चलना एक कुंजी है। प्रत्येक रामसर स्थल के लिए सामुदायिक सहभागिता योजना बननी चाहिए, जिसमें स्थानीय लोगों को वेटलैंड मित्र (Wetland Mitra) या बर्ड गार्ड जैसी भूमिकाएँ दी जा सकती हैं। इससे रोजगार भी मिलेगा और निगरानी भी बेहतर होगी। सरकार ईको-पर्यटन को बढ़ावा देते वक्त यह सुनिश्चित करे कि उससे स्थानीय लोगों को आय का स्रोत मिले – जैसे स्थानीय गाइड, होम-स्टे, हैंडीक्राफ्ट बिक्री आदि को प्रोत्साहन। इससे समुदाय संरक्षण के प्रति सहयोगी बनेंगे। शिक्षा एवं जागरूकता प्रसार भी ज़रूरी है – स्कूल पाठ्यक्रम में आर्द्रभूमि संरक्षण को शामिल करना, गांवों-कस्बों में पर्यावरण शिविर आयोजित करना तथा परंपरागत ज्ञान (Indigenous knowledge) को वैज्ञानिक प्रयासों के साथ जोड़ना चाहिए। उदाहरणस्वरूप, मणिपुर की लोकटक झील में मत्स्यपालक सहकारी समिति बनाकर स्थानीय मछुआरे मिलकर स्थायी मत्स्यन एवं जल पौधों की कटाई के नियम स्वयं लागू कर रहे हैं, जो एक अनुकरणीय मॉडल है । ऐसे मॉडलों को अन्य स्थलों पर दोहराया जा सकता है।
4. प्राकृतिक पुनर्स्थापन एवं नवाचारी उपयोग: अनेक क्षतिग्रस्त आर्द्रभूमियों को पुनर्जीवित करने की क्षमता स्वयं प्रकृति में होती है, बशर्ते मानव दबाव कम हो और थोड़ी सहायक पहल की जाए। सरकार को नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस अपनाने चाहिए – जैसे झीलों के किनारे सीवेज के प्राकृतिक उपचार हेतु रीड (reed) पट्टियाँ लगाना, प्रवाह मार्गों को बाधामुक्त करना, स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाना, जैव नियंत्रकों से जलकुंभी जैसी खरपतवार हटाना आदि । आर्द्रभूमियों का बहु-उपयोग ढूंढना भी जरूरी है – उदाहरण के लिए “निर्मल जलाशय” पहल के तहत शहरों के सीवेज का उपचार East Kolkata Wetlands जैसी प्रणालियों से किया जा सकता है; हरित अवसंरचना (green infrastructure) में wetlands को शहरी बाढ़ रोकथाम के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। सरकार को शहरी योजनाओं में अनिवार्य करना चाहिए कि महानगरों में एक न्यूनतम आर्द्रभूमि क्षेत्र संरक्षित रहे जो वर्षा जल को सोख सके। तटीय इलाकों में मैंग्रोव पुनर्स्थापन तेज करना चाहिए क्योंकि ये प्राकृतिक ढाल का काम करते हैं – जैसे सुंदरबन में बड़े पैमाने पर मैंग्रोव रोपण कर चक्रवातों के प्रभाव को कम किया जा रहा है । इन प्रकृति-आधारित उपायों से पारिस्थितिकी लाभ के साथ-साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु अनुकूलन में मदद मिलेगी।
- डाटा, शोध एवं ज्ञान-विनिमय: आज के युग में नीति निर्माण को विश्वसनीय वैज्ञानिक डाटा की आवश्यकता है। भारत को अपने प्रत्येक रामसर स्थल का दीर्घावधि वैज्ञानिक आंकड़ा संकलित करना होगा – जल की केमिस्ट्री, जैव-विविधता की प्रवृत्ति, भूमि आवरण परिवर्तन आदि। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) जैसे संस्थान पहले से कार्यरत हैं, इनका सहयोग बढ़ाया जाए। हर साइट के लिए नज़दीकी विश्वविद्यालय या कॉलेज को पर्यावरण अनुसन्धान केंद्र के रूप में जोड़ा जा सकता है, जहां के विद्यार्थी व वैज्ञानिक निरंतर अध्ययन करें। इससे Citizen Science को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोग स्वयं डाटा एकत्र करने में जुड़ेगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर Ramsar मंच पर अन्य देशों से सीखना चाहिए – जैसे ईरान में सूखती झील उर्मिया को पुनर्जीवित करने के उपाय, या जापान में शहरी wetlands का संरक्षण मॉडल। क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने से प्रवासी पक्षियों के मार्ग (flyways) की सुरक्षा के लिए तालमेल किया जा सकता है।
- नीतिगत समन्वय एवं मुख्यधारा में लाना: अंततः सबसे ज़रूरी है कि आर्द्रभूमि संरक्षण को विकास योजनाओं की मुख्यधारा में शामिल किया जाए। योजना आयोग (अब नीति आयोग) को एक स्पष्ट राष्ट्रीय आर्द्रभूमि कार्ययोजना बनानी चाहिए जिसमें संबंधित मंत्रालयों – ग्रामीण विकास, शहरी विकास, कृषि, जल संसाधन, पर्यटन, आदि – की भूमिकाएँ सुनिश्चित हों। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDGs) में भी आर्द्रभूमि संरक्षण लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल), 13 (जलवायु), 14 (समुद्री जीवन) और 15 (स्थलीय पारिस्थितिकी) का हिस्सा है , इसलिए भारत को अपने SDG रिपोर्टिंग में wetlands को प्रमुखता देनी चाहिए। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना आदि शहरी विकास कार्यक्रमों में झीलों-तालाबों के संरक्षण को KPI (मुख्य निष्पादन सूचक) बनाया जा सकता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार “राष्ट्रीय वेटलैंड्स मिशन” की स्थापना पर विचार कर सकती है जैसा कि राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना ने सुझाव दिया है, ताकि उच्च-स्तर पर निगरानी एवं मार्गदर्शन मिलता रहे।
संक्षेप में, भारत में रामसर स्थलों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम संरक्षण और विकास के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। जहाँ एक ओर रामसर टैग नए स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देकर संरक्षण की आशा जगाता है, वहीं असल सुधार स्थानीय स्तर पर लगातार प्रयास और जागरूक नीति क्रियान्वयन से ही आएगा। ऊपर बताए गए समाधानों पर ईमानदारी से अमल करते हुए भारत अपनी आर्द्रभूमियों को न सिर्फ आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रख सकेगा, बल्कि पर्यावरणीय नेतृत्व के उदाहरण भी पेश कर पाएगा।
महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु)
Q. भारत में रामसर स्थलों की संख्या संबंधी निम्न कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A. वर्ष 2025 तक भारत में कुल 91 रामसर स्थल हैं।
B. भारत रामसर स्थलों की संख्या के लिहाज़ से एशिया में प्रथम स्थान पर है।
C. तमिलनाडु राज्य में देश में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं।
उत्तर: (A), (B) और (C) – सभी सही हैं ।
Q. इनमें से कौन सा राज्य रामसर स्थल – संख्या की सही जोड़ी नहीं है?
A. तमिलनाडु – 20
B. उत्तर प्रदेश – 10
C. ओडिशा – 2
D. राजस्थान – 4
उत्तर: C. ओडिशा में 6 रामसर स्थल हैं, न कि 2 ।
Q. भारत के किन दो आर्द्रभूमि स्थलों को उनकी बिगड़ती पारिस्थितिकी के कारण मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है?
A. चिलिका झील और वुलर झील
B. केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील
C. दीपोर बील और सांभर झील
D. भोपाल की भोज वेटलैंड और पॉइंट कैलिमेरे अभयारण्य
उत्तर: B. केवलादेव (राजस्थान) और लोकटक (मणिपुर) ही भारत के दो रामसर स्थल हैं जो वर्तमान में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज हैं ।
Q. रामसर सम्मेलन के संदर्भ में “wise use” का क्या आशय है?
A. आर्द्रभूमि का वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग
B. आर्द्रभूमि का इस प्रकार उपयोग जिससे उसका पारिस्थितिक चरित्र बना रहे
C. आर्द्रभूमि का केवल स्थानीय समुदायों द्वारा उपयोग
D. आर्द्रभूमि से प्राप्त उत्पादों का बुद्धिमत्तापूर्ण विपणन
उत्तर: B. wise use का अर्थ है आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक चरित्र को बनाये रखते हुए उसका सतत विकास और उपयोग ।
Q. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
A. रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध होने पर उस आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु सरकार की प्रतिबद्धता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्ज होती है।
B. भारत ने 2022-2025 के दौरान 30 से अधिक नए रामसर स्थलों को शामिल किया है।
C. रामसर सूची में शामिल सभी आर्द्रभूमियाँ स्वतः ही राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो जाती हैं।
D. राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण आर्द्रभूमि संरक्षण से जुड़ी एक संस्थागत व्यवस्था है।
उत्तर: C. रामसर सूचीबद्ध होना किसी आर्द्रभूमि को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं देता; यह अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में पहचान मात्र है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की अलग कानूनी प्रक्रिया होती है।
Q. कौन-सा युग्म (Pair) सही सुमेलित नहीं है?
A. अमृत धरोहर योजना – आर्द्रभूमियों के स्थायी उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु हालिया पहल
B. राष्ट्रीय जलीय पारितंत्र संरक्षण योजना (NPCA) – आर्द्रभूमि व झील संरक्षण की समन्वित केंद्र-प्रायोजित योजना
C. तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) नियम – तटीय आर्द्रभूमियों को अनियंत्रित विकास से बचाने हेतु दिशा-निर्देश
D. मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड – आर्द्रभूमि पर प्रदूषण स्तर मापन की भारतीय सूचकांक प्रणाली
उत्तर: D. मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कोई भारतीय सूचकांक नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रामसर सम्मेलन की संकटग्रस्त आर्द्रभूमियों की सूची है ।
Q. भारतीय संदर्भ में ‘अमृत सरोवर’ पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था?
A. प्रत्येक जिले में 75 आर्द्रभूमियों का निर्माण/पुनर्स्थापन करना
B. 75 नए रामसर स्थलों को चिह्नित करना
C. 75 बड़ी झीलों को विश्व विरासत सूची में शामिल करना
D. 75 Wetlands को निजी क्षेत्र के सहयोग से विकसित करना
उत्तर: A. ‘अमृत सरोवर’ मिशन का लक्ष्य देशभर के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों (तालाबों/झीलों) का पुनर्जीवन/उद्धार करना था, जिसे स्वतंत्रता के 75वें वर्ष की स्मृति में प्रारंभ किया गया ।
Q. यदि किसी रामसर स्थल को Montreux Record में डाला जाता है, तो निम्न में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
A. उस स्थल को विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय फंडिंग मिली है।
B. उस आर्द्रभूमि का पारिस्थितिक चरित्र खतरे में है या बिगड़ रहा है ।
C. वह आर्द्रभूमि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन हेतु विशेष रूप से चुनी गई है।
D. उस स्थल पर रामसर टैग लागू नहीं रहेगा।
उत्तर: B. मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाले जाने का अर्थ है संबंधित रामसर स्थल के पारिस्थितिकी स्वरूप में मानव-जनित या अन्य हस्तक्षेपों के कारण नकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, अतः विशेष ध्यान की आवश्यकता है ।
Q. रामसर स्थलों के संरक्षण के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार करें:
- Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 के तहत राज्य स्तर पर आर्द्रभूमि प्राधिकरण बनाना।
- नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी बेसिन की आर्द्रभूमियों के लिए “हेल्थ कार्ड” विकसित करना।
- हर रामसर स्थल को केवल वन विभाग की जिम्मेदारी से हटाकर एक स्वतंत्र Wetland प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपना।
- राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना में आर्द्रभूमि संरक्षण को शामिल करना।
सही विकल्प चुनें:
A. केवल 1, 2 और 4 सही हैं
B. केवल 1 और 3 सही हैं
C. केवल 2 और 3 सही हैं
D. 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं
उत्तर: A. बिंदु 1, 2 और 4 सही हैं; बिंदु 3 गलत है क्योंकि वर्तमान में रामसर स्थलों का प्रबंधन संबंधित राज्य के विभाग (मुख्यतः वन विभाग) द्वारा ही किया जाता है, अलग से स्वतंत्र वेटलैंड प्राधिकरण प्रत्येक स्थल के लिए नहीं बनाया गया है।
Q. निम्न कथनों पर विचार करें:
कथन 1: भारत में किसी स्थल के रामसर सूची में शामिल होने पर वह स्थल स्वचालित रूप से कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र (जैसे वन्यजीव अभयारण्य) घोषित हो जाता है।
कथन 2: रामसर सूची में शामिल होने से उस आर्द्रभूमि को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलती है और उसके पारिस्थितिक चरित्र को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार पर आती है।
सही विकल्प चुनें:
A. केवल कथन 1 सही है
B. केवल कथन 2 सही है
C. दोनों कथन सही हैं
D. दोनों कथन गलत हैं
उत्तर: B. कथन 1 गलत है – रामसर टैग कानूनी संरक्षण का दर्जा नहीं देता, यह एक सम्मानसूचक व प्रतिबद्धतासूचक दर्जा है; कथन 2 सही है – रामसर सूची में शामिल होने पर सरकारी स्तर पर उस आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु विशेष प्रयास करने की अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी स्वीकार की जाता है ।